Book Corner हर हाथ में स्मार्टफोन के दौर में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। मगर सच यह है कि आज भी ऐसे लोगों की खासी संख्या है, जो किताबों से प्रेम करते हैं और उन्हें भी किताबों की दुनिया सजने की खबर मिलती है, वे वहां पहुंचते हैं। पहले भी और आज भी, मस्तिष्क में किसी भी संदर्भ में सामूहिकताबोध या फिर लोगों के एक जगह जमा होने से जो भाव पैदा होता है, उसका अर्थ धार्मिक या कोई सांस्कृतिक उत्सव मनाने से ही लिया जाता है। दौड़-भाग के इस समय में ऐसे जमावड़े का शुद्ध मतलब मेल-मिलाप ही माना जाता है, लेकिन बात पुस्तकों की हो, तो उसे क्या कहें- पुस्तकों का संसार या लोगों तक पहुंची पुस्तकें ? यह भी कह सकते हैं कि पुस्तकों के पीछे दर्शक – पाठक। इनके पीछे आयोजक और प्रकाशक । सबके आगे पुस्तकों की निर्बाध चाहत। जहां अलग-अलग भाषाओं की पुस्तकों के प्रेमी जुटते हैं, जहां पाठक जुड़ते हैं, पुस्तकों को छापने वाले प्रकाशक- गण एकत्रित होते हैं और लेखकों का भी जमावड़ा होता है, ऐसी ही जगहों से पुस्तक संस्कृति जीवन पाती है। मगर विडंबना यह है कि प्रचारित मेले को ही लोग मुख्य रूप से पुस्तक मेला के रूप में जानते हैं, जबकि पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति एक विस्तृत सागर है, जहां से ज्ञान अपना जीवन पाता है। लेखकों को अपनी पुस्तकों के परिदृश्य के विस्तार को अपनी आंखों से देखने में सुख मिलता है कि उनके विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं। ऐसा तब भी है, जब आज वह समय नहीं रहा, जब कभी पुस्तकें बड़ी शिद्दत से पढ़ी जाती थीं, पुस्तक – प्रेमी जब भी किताबें अपने हाथों में लिए इतराते चलते थे, तब पास-पड़ोसी तक जान जाते थे कि यह जरूर कहीं पढ़ता है।
विचारों की जगह हाथ में पुस्तकें लिए विद्यार्थी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, पर रहते छोटे बच्चे ही। स्कूल-कालेज के दिनों में कुछ बच्चे अपनी पुस्तकों में छिपा कर चिट्ठी-पाती भी किया करते थे। इसके बारे में उनके साथ वाले किसी न किसी रूप में जरूर जान जाते थे। हालांकि उनके घर वाले बेखबर हुआ करते थे। आज के युवक खुले विचारों के हैं। सोशल मीडिया ने समय को पढ़ने की अपेक्षा देखने में परिवर्तित कर दिया है। परिवर्तन बलवान ही नहीं, प्रगति के लिए भी होता है । इसलिए समय को भगवान मानते हैं। आज के प्रगतिवादी भी जमीन को देखने से पहले आसमान को देखते हैं।
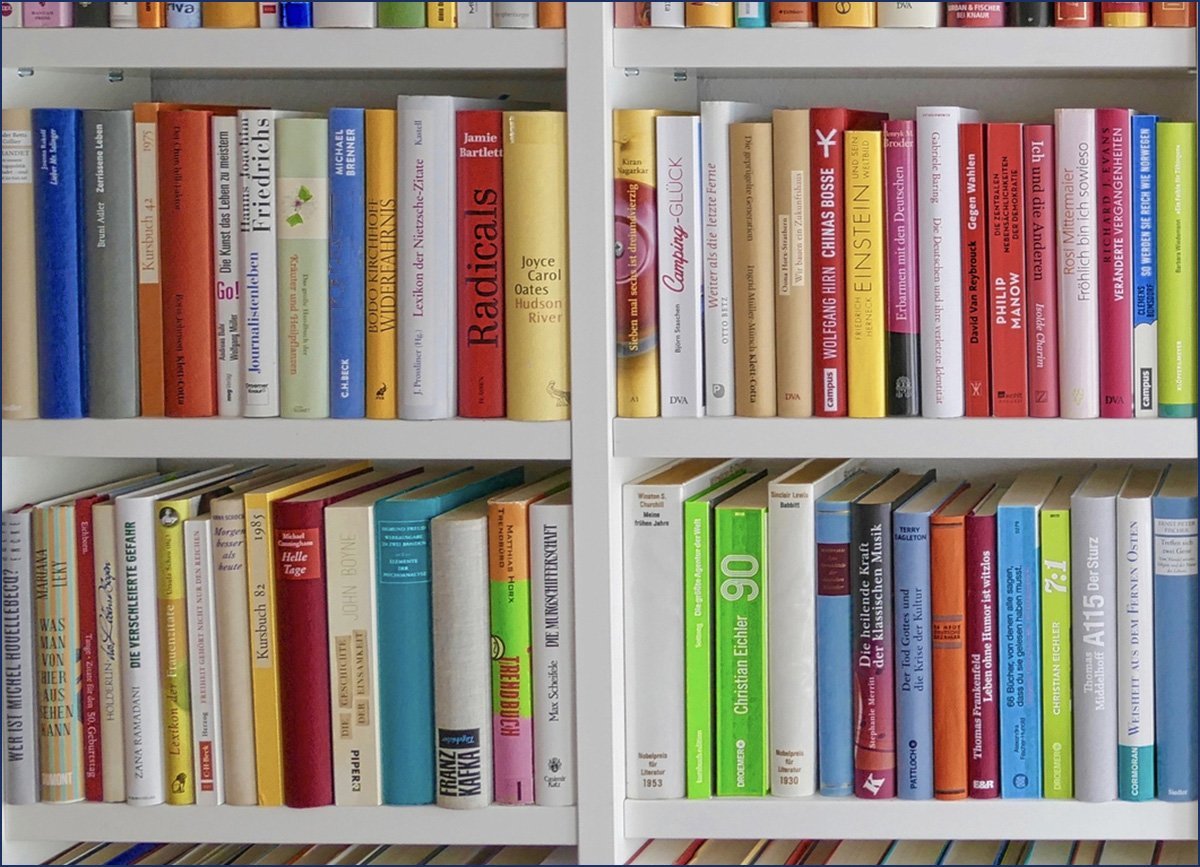
शुरू के दिनों में बच्चे पुस्तकों को देख अक्सर रोते हैं। किताबें प्रकाशित करने वालों का अलग रोना होता है। कि पुस्तकें बिकती नहीं। ऐसी स्थिति में लेखक भी यही मान लेते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त उनके पास और क्या उपाय होता है। धैर्य ही उनके लेखन की वास्तविक जननी है। इतना जानते-समझते भी पुस्तक और पढ़ने की संस्कृति के विकास के बजाय इसे आर्थिक हिसाब- किताब और मुनाफे का मौका बना लाया जाता है। यों भी सरकार किसी की हो, उसके हर फैसले को मान मिल ही जाता है, यह मान देने वाला चाहे पठन- पाठन से जुड़ा कोई भी पक्ष हो। सबकी नजरें किसी न किसी औचित्य की ओर इंगित होती हैं।
कितने लिखने वालों को इसका फल मिलता है, यह नहीं पता, लेकिन इस सबका बोझ उठाना पड़ता है पाठक को ।
रुचि का विस्तार
बहरहाल, किताबों के लिए मेल-मिलाप और एक मकसद के लिए होता है- पुस्तक-संस्कृति को जिंदा रखना । ठीक इसी तर्ज पर कभी-कभार सालाना स्तर पर आयोजन जैसे प्रयास किए जाते हैं,
ताकि पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति कम न हो। एक समान रुचि वाले लोगों के एक जगह जमा होने पर इस संस्कृति के विस्तार की संभावना पैदा होती है। लेकिन इसके समांतर यह आमतौर पर देखा जा सकता है कि अन्य अभिरुचियों के लोग भी सामूहिकताबोध की वजह से पुस्तकों के संसार में कदम रखते हैं और उसके बाद उनकी रुचि किताबों में भी विकसित होने लगती है। ऐसी जगहों पर सब तरह के लोग मिल सकते हैं। मेलजोल करने वाले भी और छत्तीस के आंकड़े वाले भी बहुत अच्छी किताबें, तो कुछ ऐसी किताबें भी, जिनको देख हैरानी हो । कितना कुछ मिल जाता है, यह पुस्तक संस्कृति से प्रेम करने वाले ही बता सकते हैं।
सहयोग की राह
करीब डेढ़ सौ करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में साक्षरता के आंकड़े के मुताबिक मोटे तौर पर कितने लोग किताबें पढ़ने वाले होंगे? जगह-जगह लगने वाले पुस्तक मेलों में यह भी मान लिया जाए कि दस करोड़ दर्शकों ने अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, तब भी प्रकाशक खुशहाल रहते हैं। दिखाने बताने को जो कहा जाए। पुस्तकें, उनके लेखकों को मिलने वाली रायल्टी आदि की बातें इतनी जटिल हैं और खासकर हिंदी की दुनिया में कि इस मसले पर बात करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। किसकी किताब किस मोड़ पर रुक जाए, कहा नहीं जा सकता। इस तरह की दुनिया में अदब का मतलब पुस्तकों के संसार में अदब से चलना होता है। इसलिए हर स्थिति में मर्यादा में रहना बुद्धिमान कहलाता है।
आवश्यकता इस बात की है कि पुस्तक – संस्कृति के विकास और विस्तार में प्रकाशकों लेखकों के हित में अगर सरकार के स्तर पर कोई ठोस कदम उठाए जाएं, तो सबसे पहले किताबें लोगों तक पहुंचाने वालों के लिए कुछ रियायत हो, ताकि बड़े के साथ-साथ छोटे प्रकाशक भी इस पुस्तक संसार में अपनी जगह बना सकें। साथ ही पुस्तकों के बढ़े डाक-शुल्क कम हों, तो सभी लोगों का भला होगा। वरना किताबों और उनकी कीमतों तक पहुंच के लिहाज से देखा जाए तो पाठकों की पुस्तकों से दूरी की वजह समझी जा सकती है। और फिर कई पुस्तकें मात्र सफेद, पीले, नीले या हरे रंग में बंट कर रह जा सकती हैं।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट, पंजाब



