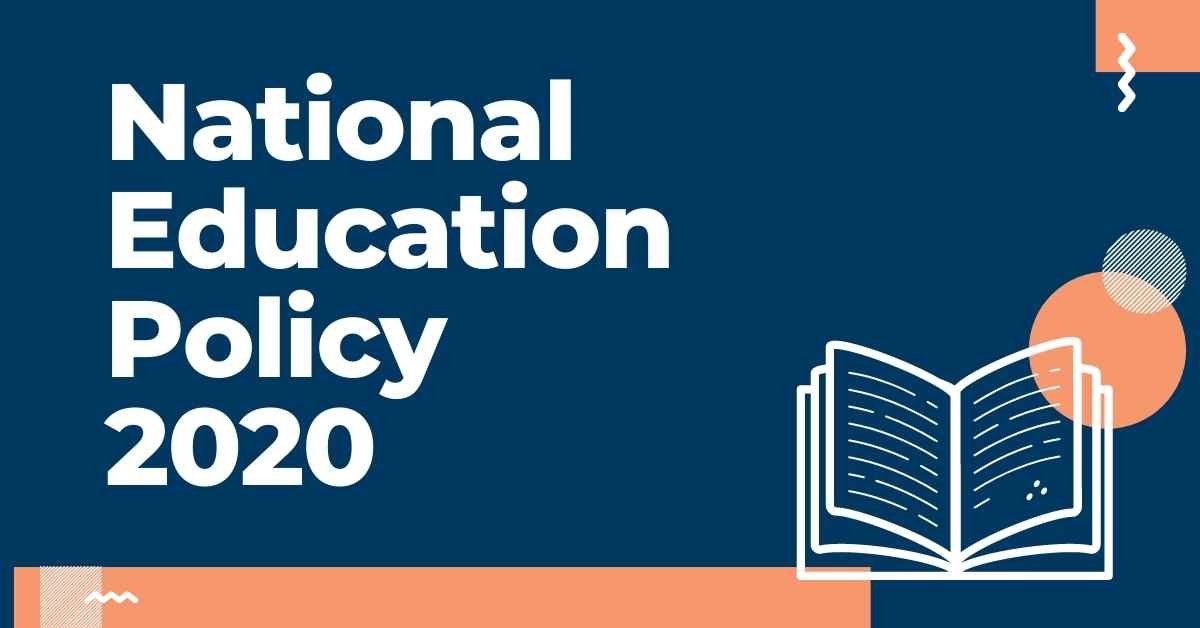The challenges in implementing the three language policy are no less राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ाने और भाषाई विविधता की सुरक्षा के उद्देश्य से त्रि-भाषा ढांचा प्रस्तुत करती है। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं और बोलियों की समृद्ध विविधता के साथ, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन हासिल करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताएँ कथित भाषाई प्रभुत्व से सम्बंधित मुद्दों और इस नीति को कार्यान्वित करने में व्यावहारिक कठिनाइयों पर ज़ोर देती हैं। त्रि-भाषा नीति का लक्ष्य बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करना है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और भारत का भाषाई परिदृश्य समृद्ध होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर भारतीय स्कूलों में तमिल पढ़ाने से सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है। बहुभाषिकता को अपनाने से न केवल संज्ञानात्मक क्षमताएँ, समस्या समाधान कौशल और रचनात्मकता बढ़ती है, बल्कि समग्र शैक्षणिक सफलता भी बढ़ती है।
अनेक भाषाओं, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता से सरकारी नौकरियों, अनुवाद और पर्यटन में विभिन्न कैरियर के रास्ते खुलते हैं। इसके अलावा, कूटनीति और बहुराष्ट्रीय निगमों में पदों के लिए बहुभाषी कौशल अक्सर आवश्यक होते हैं। नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि सीखी जाने वाली कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों, जिससे देश की भाषाई विरासत और साहित्य का संरक्षण हो सके। भारत की शास्त्रीय और क्षेत्रीय भाषाई परंपराओं को बनाए रखने के लिए संस्कृत, बंगाली, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाओं का प्रचार-प्रसार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस नीति को हिन्दी को धीरे-धीरे थोपने की नीति के रूप में देखते हैं। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए केंद्रीकृत भाषा सीखने की नीति लागू करना संघीय सिद्धांतों के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। तमिलनाडु सरकार ने एनईपी 2020 की तीन-भाषा आवश्यकता का पालन नहीं करने का विकल्प चुना है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषण में देरी हो रही है।
इसके अतिरिक्त, कई राज्यों को इन अतिरिक्त भाषाओं के लिए योग्य शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में कार्यान्वयन जटिल हो रहा है। उदाहरण के लिए, ओडिशा और केरल के स्कूलों को सीमित उपलब्धता के कारण हिन्दी शिक्षकों को ढूँढने में संघर्ष करना पड़ रहा है। अतिरिक्त भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने से भी छात्रों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे गणित जैसे आवश्यक विषयों में उनकी दक्षता प्रभावित हो सकती है। क्षेत्रीय दलों का प्रतिरोध भाषा नीतियों को अपनाने में महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। गैर-हिंदी भाषी राज्यों में राजनीतिक समूह अक्सर इन नीतियों को अपने स्थानीय शासन में घुसपैठ के रूप में देखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विरोध होता है। कई ग्रामीण छात्रों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे तीसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण बिहार में 40% छात्रों को अंग्रेज़ी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी अन्य भाषाएँ सीखने की क्षमता में बाधा आती है।
राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे केंद्रीय नीतियों के साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक ज़ोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों, संसाधनों और डिजिटल भाषा प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक धन की कमी होती है। पूर्वोत्तर भारत में तीसरी भाषा पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की कमी से प्रभावी नीति कार्यान्वयन में बाधा आती है। राज्यों के लिए एक मानकीकृत त्रि-भाषा नीति का पालन करने की बजाय अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनने की स्वतंत्रता होना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार हिन्दी लागू करने के बजाय कन्नड़, अंग्रेज़ी और विद्यार्थी की पसंद की भाषा पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ई-लर्निंग संसाधनों का विकास करना, तथा भाषा अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना स्थिति में काफ़ी सुधार ला सकता है।
आंध्र प्रदेश में डिजिटल भाषा प्रयोगशालाएँ पहले से ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थानीय भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रगति कर रही हैं। छात्रवृत्ति, कैरियर प्रोत्साहन और व्यावहारिक भाषा प्रशिक्षण की पेशकश से छात्रों को स्वेच्छा से अतिरिक्त भाषाएँ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यूजीसी संस्कृत, पाली और फारसी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे भाषाई विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार को भाषा नीति पर चर्चा में राज्यों को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संयुक्त शिक्षा समिति की स्थापना से राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक आवाज़ मिल सकेगी। मूल समस्या, शिक्षा में भाषा मानक और शिक्षण गुणवत्ता में गिरावट। कोचिंग सेंटरों ने विज्ञान और गणित में बढ़त ले ली है, तथा भाषा शिक्षा को पीछे छोड़ दिया है। यद्यपि कई सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी एक अनिवार्य विषय बन गया है, फिर भी प्रवीणता का स्तर निराशाजनक रूप से निम्न बना हुआ है।
शिक्षकों का सीमित अंग्रेज़ी कौशल सीधे तौर पर छात्रों की पढ़ाई पर प्रभाव डालता है, जैसा कि आंध्र प्रदेश में अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा की ओर बदलाव से स्पष्ट है। हिन्दी के लिए भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है; इस भाषा में शिक्षण स्तर का भी उतना ही अभाव है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को अक्सर सक्रिय शिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण के बजाय मात्र सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, पढ़ने की आदतों में गिरावट भाषा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक महत्त्वपूर्ण चुनौतियों की ओर इशारा करती है। स्कूलों में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, जिससे अंततः दीर्घकालिक भाषा कौशल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत की विविधता में एकता बनाए रखने के लिए एक समेकित भाषाई ढांचा तैयार करना आवश्यक है। भाषा के चयन में लचीलापन प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाना, तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना कार्यान्वयन सम्बंधी बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है।
अनुवाद और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भाषाई विभाजन को प्रभावी ढंग से पाट सकता है। केंद्र और राज्य के बीच सकारात्मक बातचीत और व्यावहारिक समझौता ही आगे का सबसे अच्छा रास्ता है। आपातकाल के दौरान शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसका अर्थ है कि यह एक संयुक्त जिम्मेदारी है। तीसरी भाषा से सम्बंधित विवादों के कारण समग्र शिक्षा, जो एक आवश्यक शिक्षा पहल है, के वित्तपोषण में बाधा नहीं आनी चाहिए।

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार